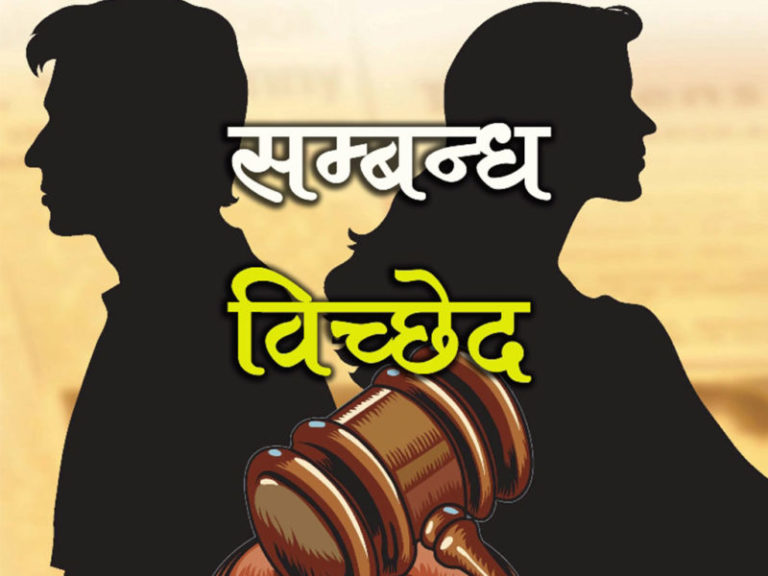दीपक चंद
भद्रपुर: झापा के कचनकबल निवासी सुमन बिक्रम संवत २०७० में विदेश में नौकरी के लिए मलेशिया गए थे। अपनी पत्नी और दो बेटियों को उनके माता-पिता के पास छोड़कर सुमन आठ साल तक वहीं रहे। इस दौरान, घर पर उनकी पत्नी और बेटियों से लगातार बातचीत होती रही। पति के माता-पिता के घर पर नहीं बनने पर, मलेशिया जाने के एक साल बाद उनकी पत्नी और बेटियाँ उनके मायके में रहने आ गईं।
मायके में रहते हुए भी, वह सुमन से लगातार बात करते रहते थे और मलेशिया से नियमित खर्च भी भेजते थे। मलेशिया छोड़ने के आठ साल बाद जब सुमन नेपाल लौटने वाले थे, तो काठमांडू हवाई अड्डे पहुँचने तक वह अपनी पत्नी के संपर्क में थे। हालाँकि, काठमांडू से झापा पहुँचने के बाद जब उन्होंने अपने मोबाइल पर उनसे संपर्क करने की कोशिश की, तो उनकी पत्नी का मोबाइल बंद था, और उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया। सुमन जब अपने घर पहुँचा, तो उसने अपनी पत्नी की माँ से संपर्क करने की कोशिश की और उसकी सास को यह कहते सुना कि उसकी बेटी उसके साथ नहीं रहती और उसे तलाक दे देना चाहिए। उसे ऐसा लगा जैसे सुमन से उसकी आधी ज़िंदगी छीन ली गई हो। आठ साल विदेश में रहने के बाद, उसकी पत्नी, जो कुछ समय से उसके नियमित संपर्क में थी, उन्होंने ने अचानक अपने १३ साल के वैवाहिक जीवन को समाप्त करने का फैसला कर लिया।
झापा के मेचीनगर की सरिता और राकेश ने अंतर्जातीय प्रेम विवाह किया था। जब उनके परिवारों ने उनके प्रेम विवाह को स्वीकार नहीं किया, तो उन्होंने भागकर एक मंदिर में शादी कर ली। शादी के बाद, उन्होंने मज़दूरी की और बाज़ार में एक कमरा किराए पर लिया। शादी के दो साल बाद, उनके बेटे का जन्म हुआ। बेटे के जन्म के बाद, राकेश के परिवार ने सभी को अपने घर बुलाया।
घर बुलाए जाने के एक महीने के भीतर ही सरिता को तरह-तरह की यातनाओं का सामना करना पड़ा। राकेश के परिवार ने उसे मानसिक तनाव देना शुरू कर दिया, जैसे कि यह कहना कि वह घर का सारा काम करती है, कुछ नहीं करती, वह काम करने में अच्छी नहीं है, वह किसी की बेटी है, और उन्होंने उसे कुछ नहीं सिखाया। राकेश, जो उससे प्यार करता था और उससे प्यार करता था, धीरे-धीरे अपने व्यवहार में भी बदलाव लाने लगा। अपने परिवार के उकसावे में आकर राकेश भी शराब पीकर उसके साथ दुर्व्यवहार करने लगा, उसे मारने-पीटने लगा, उसे खाना नहीं देने दिया और अत्यधिक यातनाएँ देने लगा।
जब राकेश और उसके परिवार का अत्याचार चरम पर पहुँच गया, तो इसे सहन न कर पाने के कारण सरिता ने अपने रिश्तेदारों की मदद से अदालत में तलाक का मुकदमा दायर कर दिया। अदालत ने दोनों को मध्यस्थता के लिए एक मध्यस्थ के पास भेज दिया। जिस घर में वे मिलने के लिए सहमत हुए थे, वहाँ पहुँचने के २-३ दिन बाद, सरिता ने आखिरकार हिस्से के साथ तलाक की अपील की।
ये तो बस दो उदाहरण हैं। ऐसी कई घटनाएँ अब देश के हर शहर और गाँव में दोहराई जा रही हैं। नेपाल जैसे पारंपरिक समाज में, जो पारिवारिक संबंधों को प्राथमिकता देता है, विवाह को एक ‘अटूट बंधन’ और ‘पवित्र रिश्ता’ माना जाता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इस पारंपरिक सोच में बड़ा बदलाव आया है। ऐसे पति-पत्नी की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है जो अपनी शादी को बरकरार न रख पाने और एक-दूसरे के साथ न रह पाने की स्थिति में तलाक के लिए तैयार हो जाते हैं। तलाक, जिसे एक दशक पहले एक दुर्लभ घटना माना जाता था, अब रोज़ाना समाचारों में सुना, पढ़ा और देखा जा सकता है।
यह प्रवृत्ति हमारे समाज में नई तरह की सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, कानूनी और आर्थिक समस्याएँ पैदा कर रही है। वित्तीय वर्ष बिक्रम संवत २०८०/८१ के लिए सुप्रीम कोर्ट की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, अदालतों में सबसे ज़्यादा दायर मामला तलाक का था। उस वित्तीय वर्ष में, ४०,३२० लोगों ने वैवाहिक संबंध समाप्त करने के लिए मामले दायर किए। इस आँकड़ों पर गौर करें तो नेपाल की अदालतों में हर दिन औसतन ११० से ज़्यादा लोग तलाक के लिए आवेदन करते हैं।
झापा ज़िला न्यायालय के आँकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष २०८१/८२ में १,३४३ लोगों ने तलाक के लिए मामले दायर किए। इस आँकड़ों के अनुसार, झापा ज़िले में औसतन हर दिन चार लोग अपने वैवाहिक संबंध समाप्त करना चाहते हैं। हाल ही में, झापा ज़िला सबसे ज़्यादा तलाक़ वाले प्रमुख ज़िलों में शामिल रहा है।
सामाजिक कार्यकर्ता दयानंद गोस्वामी कहते हैं कि विदेश में रोज़गार, सोशल मीडिया का दुरुपयोग और तकनीक का अनियंत्रित इस्तेमाल तलाक़ के मुख्य कारण हैं। जब पति या पत्नी लंबे समय तक विदेश में रहते हैं, तो पारिवारिक रिश्ते कमज़ोर हो जाते हैं। सोशल मीडिया के ज़रिए नए रिश्ते की शुरुआत, किसी दूसरे व्यक्ति से मिलना या ऑनलाइन आकर्षण बढ़ना भी शादियों में खलल डाल रहा है। खासकर ग्रामीण इलाकों में, तलाक के बाद भी महिलाओं को ही दोषी ठहराया जाता है। इससे ऐसी स्थिति पैदा होती है जहाँ दोबारा शादी करना मुश्किल होता है और परिवार व समाज में स्वीकृति पाना मुश्किल होता है। खस क्षेत्री समाज के अध्यक्ष खड़ग बहादुर खड़का कहते हैं, “नेपाल जैसे पारंपरिक समाज में तलाक को न केवल व्यक्तिगत, बल्कि सामूहिक कलंक के रूप में भी देखा जाता है।”
एडवोकेट नरेश खाती कहते हैं, “देश के नागरिक संहिता, २०७४ ने दोनों पक्षों को तलाक का समान अधिकार दिया है, लेकिन व्यवहार में यह आसान नहीं है। कानूनी प्रक्रिया लंबी और महंगी है, और समाज में नकारात्मक मानसिकता प्रबल है। इसलिए, पीड़ित अदालत जाने से हिचकिचाते हैं।” एडवोकेट खाती कहते हैं कि स्टडी या डिपेंडेंट वीज़ा पर विदेश में शादी करने और फिर वहाँ पहुँचकर तलाक लेने के मामले भी बढ़े हैं। एक और दिलचस्प तथ्य यह है कि हाल के दिनों में ४० साल से ज़्यादा उम्र के लोगों में तलाक ज़्यादा आम है।
तलाक के बाद दोनों पक्ष मानसिक रूप से आघातग्रस्त होते हैं। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा असर बच्चों पर पड़ता है। वे असुरक्षित, असुरक्षित और कभी-कभी आक्रामक हो सकते हैं। इसलिए, तलाक को न केवल एक कानूनी प्रक्रिया होना चाहिए, बल्कि इसे मनोवैज्ञानिक उपचार से भी जोड़ा जाना चाहिए, ऐसा भद्रपुर नगर पालिका की उप- मेयर राधा कार्की कहती हैं। उनका कहना है कि हालाँकि तलाक व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में यह स्वतंत्रता की सीमाओं को लांघ जाता है। अक्सर, तलाकशुदा बच्चे अकेलेपन का अनुभव करते हैं और धीरे-धीरे नशे की लत में पड़ जाते हैं। उप-मेयर कार्की का कहना है कि आर्थिक लाभ, संयुक्त परिवार में न रह पाने आदि के कारण होने वाले तलाक समाज के लिए हानिकारक हैं।
पत्रकार नेत्र बिमली कहती हैं कि जो महिलाएँ हमारे घर-समाज से उन देशों में चली गई हैं जहाँ वे विदेशी नौकरियों में अच्छा पैसा कमाती हैं, अक्सर अच्छी आय अर्जित करने के बाद तलाक ले लेती हैं। उनका कहना है कि तलाक के कुछ मामले तब भी बढ़ रहे हैं जब माता-पिता अपने बच्चों को अच्छी सलाह नहीं देते।
सामाजिक कार्यकर्ता दयानन्द गोस्वामी का कहना है कि तलाक का हमारे समाज पर बहुआयामी प्रभाव पड़ रहा है। इसका सीधा असर सबसे पहले बच्चों पर पड़ता है। माता-पिता के अलग होने के बाद, बच्चों में आत्मविश्वास की कमी होती है, उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है और उन्हें समाज में आसानी से घुलने-मिलने में मुश्किल होती है। कुछ मामलों में, उनमें आपराधिक प्रवृत्तियाँ या गहरी मानसिक समस्याएँ भी विकसित हो जाती हैं। इसी तरह, तलाक के बाद भी समाज महिलाओं पर बहुत दबाव डालता है। खासकर ग्रामीण इलाकों में, तलाकशुदा महिलाओं को दोषी ठहराने का चलन अभी भी जारी है। वे कहते हैं कि इसके कारण, उन्हें न केवल पुनर्विवाह करने में कठिनाई होती है, बल्कि अपने परिवार और समाज में स्वीकृति पाने में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पत्रकार देवेंद्र किशोर ढुङगाना कहते हैं कि संयुक्त परिवारों के विघटन के कारण तलाक का चलन बढ़ने लगा है। ढुङगाना कहते हैं, “हमारे परिवार से प्यार टूट गया है, लेकिन हम एक कुत्ते से प्यार कर रहे हैं। पत्रकारिता को ऐसे मुद्दों को ज़िम्मेदारी से उठाना चाहिए। अगर तलाक बड़ी मात्रा में एक समस्या है, तो छोटी मात्रा में यह एक समाधान भी है।” तलाक को दो पहलुओं से देखा जा सकता है। एक तरफ, यह एक गहरी समस्या है जो परिवारों को तोड़ती है, बच्चों के भविष्य में अंधकार लाती है, महिलाओं पर सामाजिक कलंक लगाती है और सामाजिक ढांचे को ही कमज़ोर करती है। दूसरी ओर, कई पीड़ितों के लिए, तलाक मुक्ति का एक साधन और समाधान है—रोज़मर्रा की हिंसा, यातना और असमान रिश्तों से बाहर निकलने का एक कानूनी रास्ता है।
इस प्रकार, तलाक को केवल एक समस्या के रूप में नकारात्मक रूप से नहीं देखा जा सकता। यदि वैवाहिक संबंध अस्वस्थ, असमान और हिंसक हैं, तो ऐसे रिश्ते को जबरन बनाए रखना और भी बड़ी समस्या है। हालाँकि, लापरवाही, आवेग या तकनीक के दुरुपयोग के कारण एक स्वस्थ रिश्ते का टूटना समाज के लिए एक गंभीर चुनौती है।
इसलिए, यह समझना आवश्यक है कि तलाक एक समस्या भी है और समाधान भी। इसका सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव परिस्थितियों, कारणों और परिणामों पर निर्भर करता है। दीर्घावधि में, समाज को इसे समस्या-केंद्रित दृष्टिकोण से अधिक समाधान-उन्मुख दृष्टिकोण में बदलना होगा, जहाँ ऐसा वातावरण बनाया जाए जहाँ तलाक के बाद भी बच्चे के अधिकार, सम्मान और भविष्य की रक्षा हो।